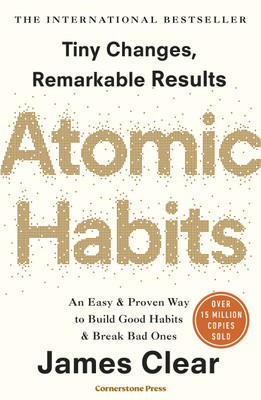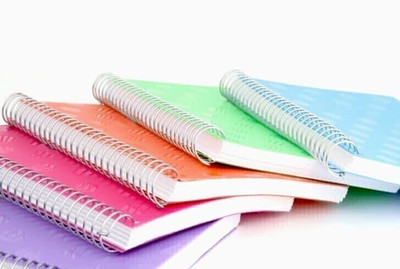नागफनी (व्यंग संग्रह) राजेश दुबे एंड डॉ आनंद प्रकाश त्रिपाठी (हार्डकवर, राजेश दुबे एंड डॉ आनंद प्रकाश त्रिपाठी)
Share
नागफनी (व्यंग संग्रह) राजेश दुबे एंड डॉ आनंद प्रकाश त्रिपाठी (हार्डकवर, राजेश दुबे एंड डॉ आनंद प्रकाश त्रिपाठी)
इस प्रोडक्ट पर राय देने वाले पहले व्यक्ति बने
ख़ास कीमत
₹248
₹250
आपके लिए कूपन
T&C
उपलब्ध ऑफ़र
T&C
T&C
T&C
T&C
Delivery
Check
Enter pincode
डिलीवरी2 मई, शुक्रवार|₹65
?
जानकारी देखें
Highlights
- लेखक: राजेश दुबे एंड डॉ आनंद प्रकाश त्रिपाठी
- 184 पेज
- पब्लिशर: अनुग्या बुक्स
सर्विस
- कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध?
Seller
जानकारी
किसी के माथे पर उगी चिन्ताओं की लकीरों को मिटते हुए देखना सुख देता है। जब मैं अपने आस-पास के आदमियों को, आधारभूत सुविधाओं के अभाव में तड़पते और बेहाल देखता हूँ तो व्यवस्थाओं के प्रति मन क्षुब्ध हो जाता है और जिम्मेवार लोगों के प्रति घृणा जागने लगती है। यह तो हमारे आस-पास की हकीकत है। बाकी तो उच्च स्तरीय अव्यवस्थायें हैं, जो स्वार्थों की गहरी नींव पर खड़ी हैं, जहाँ काजल की कोठरी का सुख भोगते भाग्यवान, निरापद हैं। इसी चिन्ता के साथ हम छोटे से बड़े हुए हैं। हम अपनी इन परिस्थितियों की कीचड़ में धँसे अपने हाथ-पाँव तक ना हिलाये, डुलाये और उबरने की जुगत बनायें, यह कैसे हो सकता है पर यह हो रहा है। हम अपनी वर्तमान चिन्ताओं को ना पहचान पायें, ना जान पायें ऐसा दुराग्रह, हमें तर्कहीन उत्सव मनाने के लिए बाध्य करते हैं। ये शासकीय आयोजन, ये प्रायोजित खेल उत्सव, आदमी को भटकाव की अन्धी गलियाँ हैं, जहाँ भटकता जन अपने भाग्य को कोसता रहता है। जो कुछ हँसकर, कुछ मुस्कुराकर, कुछ झल्लाकर, कुछ हास्य से, कुछ विनोद से व्यक्त करती है। पर जो कुछ भी है वह सब मेरी चिन्ता के आस-पास है। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए मैंने आम आदमी के दु:खों, तकलीफों, उनकी चिन्ताओं को बहुत नजदीक से देखा, जाना, परखा है। आज भी हमारा किसान और मजदूर-वर्ग वैसा ही जीवन जी रहा है जैसे प्रेमचन्द के पात्र भोग रहे थे। आज भी घीसू, माधव, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया मिलते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। वे आज भी वैसे ही दु:खी हैं। वे आज भी वैसे ही सुखी हैं। समयानुसार अन्तर आया है तो सिर्फ इतना कि झोपडिय़ों में कुछ थूनिया लगा दी गयी हंै जो झोंपड़ी को जमीदोंज होने से बचा रही है। देहातों में इमारतों के जंगल उग आये हैं। आज भी शोषण की परिस्थितियाँ और शोषण की कुटिल मनोवृत्तियाँ पूर्ववत् कायम हैं।
Read More
Specifications
| बुक |
|
| ऑथर |
|
| बाइंडिंग |
|
| पब्लिशिंग की तारिख |
|
| पब्लिशर |
|
| नंबर ऑफ पेज |
|
| लैंग्वेज |
|
Manufacturing, Packaging and Import Info
Safe and Secure Payments.Easy returns.100% Authentic products.
Back to top